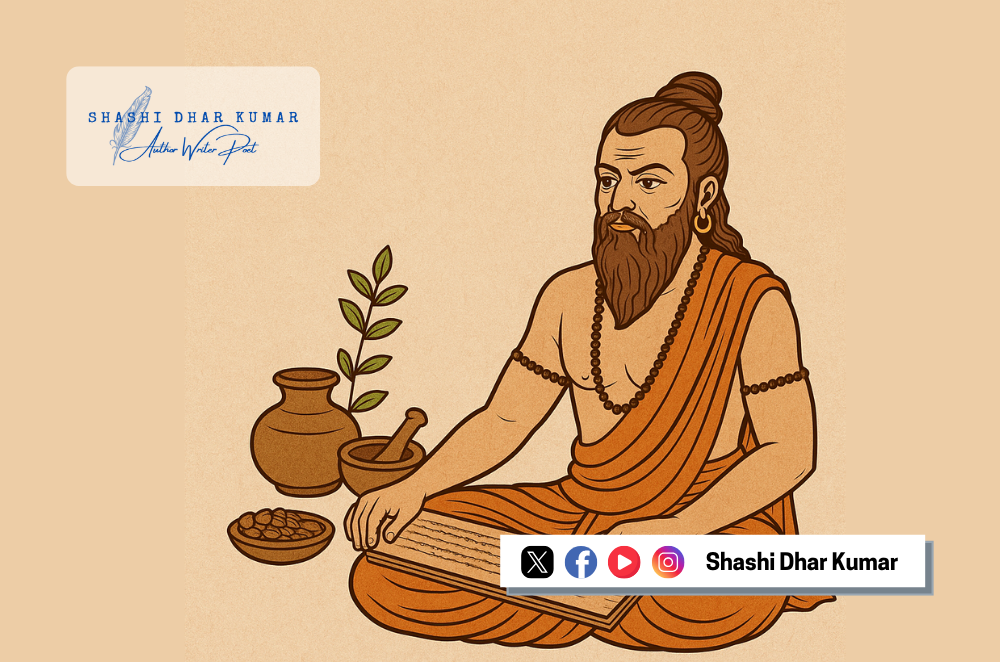
महर्षि चरक – आयुर्वेदिक उपचार विज्ञान के शाश्वत स्तंभ
- Shashi Dhar Kumar
- 23/07/2025
- लेख
- आयुर्वेदिक, उपचार विज्ञान, महर्षि चरक
- 0 Comments
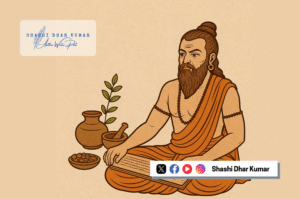 भारतीय चिकित्सा परंपरा का आधारभूत स्तंभ “आयुर्वेद” न केवल शारीरिक उपचार की प्रणाली है, बल्कि यह जीवन को दीर्घायु, स्वस्थ और संतुलित बनाने का शास्त्र भी है। इस प्राचीन विज्ञान के सूत्रधारों में महर्षि चरक का स्थान सर्वोच्च है। उन्होंने चिकित्सा विज्ञान को औषधि, आहार, दिनचर्या, मनोविज्ञान और नीतिशास्त्र के साथ जोड़कर इसे समग्र जीवन-दर्शन का रूप प्रदान किया।
भारतीय चिकित्सा परंपरा का आधारभूत स्तंभ “आयुर्वेद” न केवल शारीरिक उपचार की प्रणाली है, बल्कि यह जीवन को दीर्घायु, स्वस्थ और संतुलित बनाने का शास्त्र भी है। इस प्राचीन विज्ञान के सूत्रधारों में महर्षि चरक का स्थान सर्वोच्च है। उन्होंने चिकित्सा विज्ञान को औषधि, आहार, दिनचर्या, मनोविज्ञान और नीतिशास्त्र के साथ जोड़कर इसे समग्र जीवन-दर्शन का रूप प्रदान किया।
महर्षि चरक
चरक का काल निर्धारण इतिहासकारों में विवाद का विषय रहा है, परन्तु सामान्यतः उन्हें लगभग ईसा पूर्व प्रथम या द्वितीय शताब्दी का माना जाता है। वह “आत्रेय पद्धति” के प्रमुख अनुयायी थे। “चरक संहिता” नामक ग्रंथ के रचयिता माने जाने वाले महर्षि चरक ने औषध शास्त्र और चिकित्साशास्त्र को वेदों और उपनिषदों से जोड़कर एक तात्त्विक आयाम प्रदान किया।
चरक संहिता: आयुर्वेद का मूल स्रोत
“चरक संहिता” आयुर्वेद के तीन प्रमुख ग्रंथों (बृहत्त्रयी) में से एक है, अन्य दो हैं – सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम्। चरक संहिता में आठ अंगों (अष्टांग आयुर्वेद) का विस्तार मिलता है:
1. काय चिकित्सा
2. बाल चिकित्सा (कौमारभृत्य)
3. भूत-विद्या
4. शालाक्य तंत्र
5. शल्य तंत्र
6. अगद तंत्र
7. रसायन तंत्र
8. वाजीकरण तंत्र
महर्षि चरक की चिकित्सा-दृष्टि
चरक संहिता में रोग का मूल कारण “त्रिदोष सिद्धांत” (वात, पित्त, कफ) को माना गया है। जब ये दोष सम स्थिति में होते हैं, तब व्यक्ति स्वस्थ होता है और जब असंतुलित होते हैं, तब रोग उत्पन्न होते हैं। चरक का दृष्टिकोण केवल औषधि पर आधारित नहीं था, बल्कि उन्होंने मन, आचार, आहार और वातावरण को भी रोग के कारणों में गिना।
मुख्य अवधारणाएँ:
1. स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा –
चरक संहिता (सूत्रस्थान 9.4) में लिखा है:
“समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः ।
प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥”
अर्थात जिसके दोष, अग्नि, धातु और मल की क्रियाएं सम होती हैं तथा आत्मा, इन्द्रियां और मन प्रसन्न रहते हैं, वही स्वस्थ कहलाता है।
2. निदान पंचक – रोग का निदान पाँच प्रमुख तरीकों से किया जाता है:
हेतु (कारण)
पूर्वरूप (पूर्व लक्षण)
रूप (मुख्य लक्षण)
उपशय (रोग में राहत देने वाली चीज़ें)
सम्प्राप्ति (रोग की गति)
3. औषधि सिद्धांत – औषधि का गुण, रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव को ध्यान में रखकर उपचार दिया जाता था।
4. रसायन और वाजीकरण – चरक ने रसायन (टॉनिक) और वाजीकरण (प्रजनन क्षमता बढ़ानेवाली औषधियाँ) पर भी विस्तृत लेखन किया, जिससे आयु, स्मृति, बल और ओज की वृद्धि हो।
चरक संहिता में औषधियों का वर्गीकरण
चरक ने औषधियों को उनके प्रभाव और गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बाँटा। उदाहरण के लिए:
दीपन-पाचन औषधियाँ – जैसे पिप्पली, हिंगु
शीतल औषधियाँ – जैसे चंदन, शतावरी
रसायन औषधियाँ – जैसे अमलकी (आंवला), हरितकी (हरड़)
वाजीकरण औषधियाँ – जैसे अश्वगंधा, कुष्ठ
चरक और चिकित्सा नैतिकता
चरक संहिता में चिकित्सक के आचार-संहिता पर विशेष बल दिया गया है। उन्होंने कहा – “वैद्य वही उत्तम है जो रोग को पूरी तरह समझे, अपने कार्य में दक्ष हो, सत्य बोले, संयमी हो, और धन के प्रति लोभी न हो।”
चरक संहिता (विमानस्थान 8.13) में लिखा है: “आत्मविज्ञानं चिकित्सायां प्रधानं – अर्थात एक अच्छा वैद्य पहले स्वयं को जाने।”
चरक की वैश्विक मान्यता
चरक का कार्य केवल भारत में ही नहीं, अपितु विश्व के प्राचीन चिकित्साविज्ञान में भी आदर से उद्धृत होता रहा है। यूनानी और तिब्बती चिकित्सा पद्धतियों पर भी चरक संहिता का प्रभाव देखा गया है।
महर्षि चरक केवल एक औषधि विज्ञानी नहीं, बल्कि आयुर्वेद को समग्रता में समझने वाले दार्शनिक थे। उन्होंने मनुष्य के जीवन, मन, शरीर और ब्रह्मांड के बीच संतुलन को चिकित्सा का मूलाधार बनाया। आज के युग में जब चिकित्सा केवल शारीरिक लक्षणों पर केंद्रित हो गई है, चरक की समग्र दृष्टि और सिद्धांत पुनः प्रासंगिक हो उठते हैं।
©️✍️शशि धर कुमार, कटिहार, बिहार
Instagram ID: ishashidharkumar
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.

